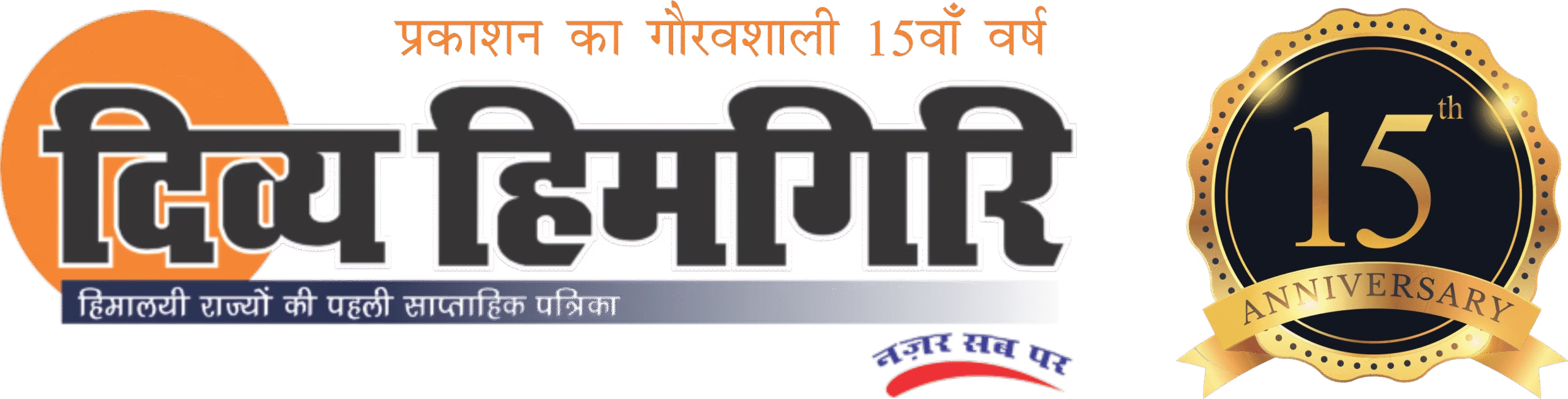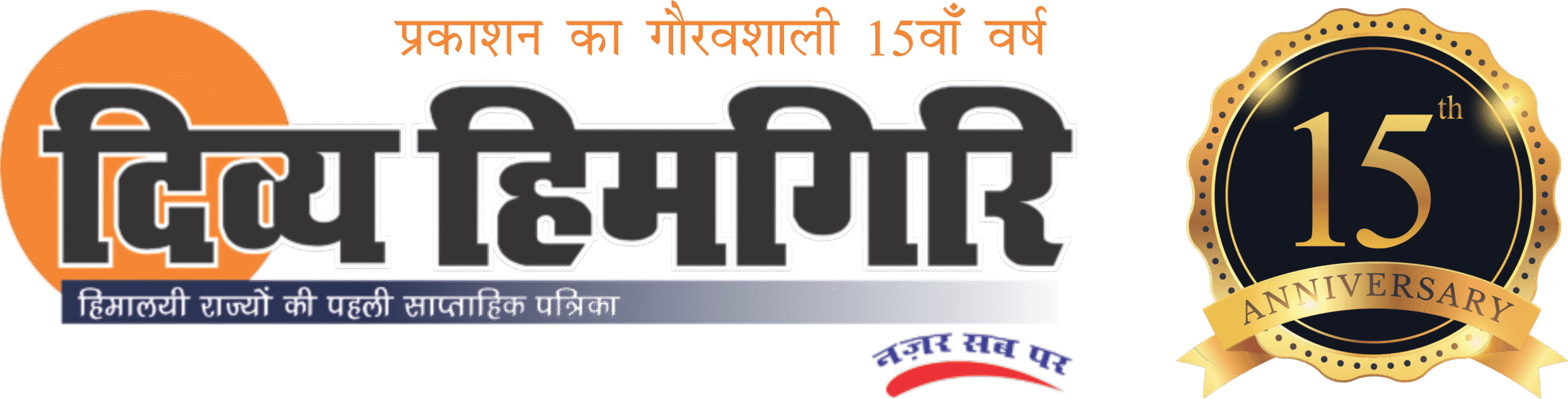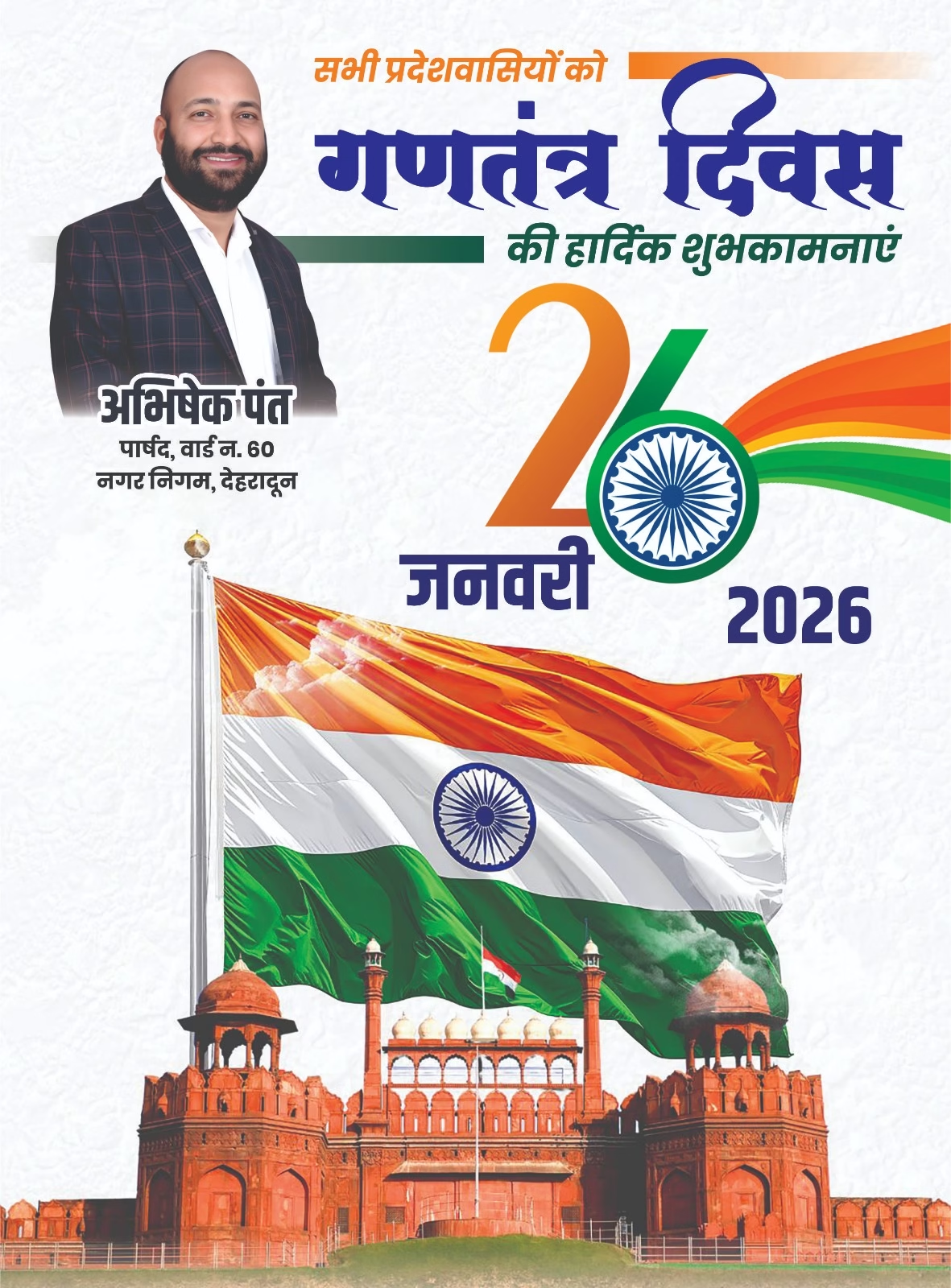पारंपरिक चिकित्सा सदैव से स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में घरों और समुदायों में अभिन्न संसाधन के रूप में रही है। यह चिकित्सा स्वदेशी पद्धतियों के साथ विभिन्न देशों और संस्कृतियों में समय के साथ-साथ पोषित होकर सामान्य जन-मानस के स्वास्थ्य को बनाए रखने, शारीरिक और मानसिक बीमारी को रोकने, निदान तथा उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। दूसरे शब्दों में पारम्परिक चिकित्सा शब्द ज्ञान, कौशल और प्रथाओं का कुल योग है। भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों ‘आयुष’ के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। वर्ष 1995 में स्थापित भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग, वर्ष 2003 से आयुष मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धति जैसे सि(ा, यूनानी, नेचुरोपैथी ;प्राकृतिक चिकित्साद्ध अपने विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। विश्व के 170 देशों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग की जानकारी दी गई है, जिसमें एक्यूपंक्चर का अभ्यास 113 देशों में सबसे आम है। कई अन्य विकसित देशों ने पारंपरिक चिकित्सा को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में मान्यता देना और एकीकृत करना शुरू कर दिया है।
भारतीय पारम्परिक चिकित्सा का प्रादुर्भावः
भारत को कई मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियों का अनूठा गौरव प्राप्त है। वैदिक काल में अश्विनी कुमार जिन्हें ‘अश्विनौ’ अर्थात दो अश्विनों का उल्लेख है, को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। जिनके हाथ में मधुकलश है। )गवेद में 376 बार इनका वर्णन है, जो 57 )चाओं में संग्रहित है। वही स्थान पौराणिक काल में भगवान धन्वन्तरी को मिला है, जिनके हाथ में अमृत कलश है। धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है, जो सबकी रक्षा करते हैं। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा से जुडे वैद्य इन्हें आरोग्य का देवता मानते हैं, जिन्होंने अमृतमय औषधियों की खोज की थी। दिवोदास धन्वंतरी के वंशज थे, जिन्होंने विश्व के पहले शल्य चिकित्सा विद्यालय की शुरूआत काशी में की थी। महर्षि विश्वामित्रा के पुत्रा और दिवोदास के शिष्य सुश्रुत को इस विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था, जा सदियों से एकत्रित और पोषित पौराणिक ज्ञान से दो प्रमुख स्कूल और आठ विशेषज्ञताएं विकसित हुईं थी। एक चिकित्सकों का स्कूल था, जिसे धन्वन्तरी सम्प्रदाय या परम्परा के ‘चरक संहिता’ तो दूसरा स्कूल सर्जनों ;शल्य चिकित्सकोंद्ध को आत्रोय सम्प्रदाय के ‘सुश्रुत संहिता’ के रूप में पौराणिक साहित्य में प्रतिनिधित्व और संदर्भित किया गया है। भावप्रकाश के अनुसार आत्रोय आदि मुनियों ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उसे अग्निवेश तथा अन्य शिष्यों को दिया था। 1885 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पश्चिमी चिकित्सा का प्रभुत्व अपने चरम पर पहुंच गया, जब लाॅर्ड मैकाले ने पूर्वी भारत कम्पनी द्वारा शासित सभी क्षेत्रों में पश्चिमी ज्ञान को प्रोत्साहन देने के आदेश दिए थे। भारतीय राष्ट्रवाद की शुरूआत के साथ 20वीं सदी में कला और विज्ञान में पिफर से लोगों की अभिरुचि जाग्रत हुई, और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का धीरे-धीरे पुनर्जागरण शुरू हुआ। भारत सरकार ने 1969 में स्वदेशी चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी पर एक केंद्रीय परिषद की स्थापना की। 1978 में इसे चार अलग-अलग परिषदों (1) केंद्रीय आयुर्वेद और सि( में अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) (2) केंद्रीय होम्योपैथी में अनुसंधान परिषद (3) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान परिषद तथा (4) केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान परिषद में विभाजित किया गया। भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा प(ति ;आईएसएमद्ध के संबंध में कार्रवाई के तरीके पर सलाह देने के लिए भोरे समिति और मुदालियर समिति जैसी कई उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया। चोपड़ा रिपोर्ट ने भारतीय चिकित्सा प(ति और आधुनिक चिकित्सा पर पूर्ण एकीकरण की सिपफारिश की, परंतु स्वास्थ्य देखभाल में ऐलोपैथिक पेशेवरों के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में स्वदेशी चिकित्सकों को शामिल करने में सिपफारिशों का पालन नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ;1983द्ध में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में आईएसएम को महत्वपूर्ण भूमिका मिली और 1995 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा प(ति और होमियोपैथी ;आईएसएम और एचद्ध का एक अलग विभाग बनाया गया। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ;संशोधनद्ध विधेयक में, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 में संशोधन करने के बाद 09 अगस्त, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। वर्तमान में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की ताकत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। भारतीय सभ्यता और परम्पराऐं जो कभी सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त थी, का क्रमब( संजोया हुआ इतिहास होते हुए भी उसकी उपयोगिता और उपलब्धता से लोग अनभिग्य हैं। उपलब्ध जानकारियों से बहुत कुछ समझने की कोशिश तो की जाती है, परंतु विभिन्न भाषाओं में उनका रूपांतरण ना मिलने, व्यापक शोध की कमी, सरल रूप में समझने और आधुनिक विद्वता के साथ तालमेल में असमंजतता के प्रति एक मजबूत प्रयास की जरूरत दिखाई देती है। भौतिक सनातन संस्कृति, ब्रह्माड ;खगोलीयद्ध विज्ञान की प्रारम्भिक संकल्पनाओं, खगोल शास्त्रा से विक्रम सम्वत या भारतीय पांचाग से समय की गणना या गणितीय माॅडल के आधार का विकास या पिफर नालन्दा जैसे शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्रों से उपजे ज्ञान से अरब में हिजरी सम्वत और यूरोप में जूलियन पांचाग के आधार पर परिष्कृत और संशोधित हुए कैलेंडर या ज्ञान आज भी उपलब्ध हैं। परंतु अवलोकन के आधार पर खगोलीय ज्ञान को 1500 के दशक में निकोलस कोपरनिकस द्व ारा की गई ब्रह्माड के विज्ञान की शुरूआत, 1600 के दशक में न्यूटन के ‘सेब के गिरने से ग्रेविटी का सि(ांत, 1700 के दशक में बेंजामिन प्रफेंकलिन के पतंग उडाने से ‘तडित बिजली का सि(ांत’ या पिफर 20वीं सदी की शुरूआत में अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षता के सिं(ात आदि से ही भौतिक के नियम प्रतिपादित हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में इस प्राचीनतम बहमूल्य ज्ञान को विकास का आधार ना मानने का एक बडा प्रमुख कारण वैश्विक समुदाय में विभिन्न मतांतर, शिक्षा को भारतीय संस्कृति से जोडने या पिफर वैश्विक स्तर पर अनुपलब्धता से यह ज्ञान सिमटा हुआ सा दिखाई देता है। हालांकि, भारतीय चिकित्सा प(ति को ऐशियाई देशों ने सहर्ष स्वीकारा है, जिसका वैश्विक प्रतिरूप इस केंद्र के माध्यम से कई देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित दिखाई देता है। आयुष चिकित्सा प्रणालियों का सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक प्रभाव के कारण आयुर्वेद और योग को मुख्यतः संस्कृत और हिंदी भाषाओं में, जबकि यूनानी, सि(ा आदि को उर्दू या फ़ारसी में शुरूआत में अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षता के सिं(ात आदि से ही भौतिक के नियम प्रतिपादित हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में इस प्राचीनतम बहमूल्य ज्ञान को विकास का आधार ना मानने का एक बडा प्रमुख कारण वैश्विक समुदाय में विभिन्न मतांतर, शिक्षा को भारतीय संस्कृति से जोडने या पिफर वैश्विक स्तर पर अनुपलब्धता से यह ज्ञान सिमटा हुआ सा दिखाई देता है। हालांकि, भारतीय चिकित्सा प(ति को ऐशियाई देशों ने सहर्ष स्वीकारा है, जिसका वैश्विक प्रतिरूप इस केंद्र के माध्यम से कई देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित दिखाई देता है। आयुष चिकित्सा प्रणालियों का सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक प्रभाव के कारण आयुर्वेद और योग को मुख्यतः संस्कृत और हिंदी भाषाओं में, जबकि यूनानी, सि(ा आदि को उर्दू या पफ़ारसी में पढाया जाता है, या पिफर उत्तीर्ण करना पडता है। आयुर्वेद एक प्रमुख प्रणाली होने के कारण अन्य प्रणालियों के अस्तित्व से आगे निकल जाती है, जो किसी न किसी रूप में निरंतर अपवाद का कारण बनकर कठघरे में खडी की जाती है। दिसम्बर 2004 में जर्नल आॅपफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित शोध में आयुर्वेदिक दवाओं में सीसा, पारा और/या आर्सेनिक के संभावित हानिकारक स्तर के होने की खबर दी गई थी। हाल ही में शु(ता और प्रमाणिकता के दावे पर भी सवाल उठाए गए हैं। अतः पारंपरिक चिकित्सा को आदर्श नहीं बनाना चाहिए बल्कि सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत में भाषाई अभिरूचि की वजह से भी इनका एकीकरण या आधुनिकीकरण कर पाना बहुत सम्भव नहीं हो पाया है। इसलिए आयुष प्रणालियों की शिक्षा को भाषाओं की सीमाओं से मुक्त करने की आवश्यकता है। पारम्परिक चिकित्सा के क्षेत्रों में कम गुणवत्ता वाली शिक्षा और आयुष विद्यालयों की भरमार सी हो गई है, तथा पारम्परिक चिकित्सा शिक्षा का आधुनिकीकरण अपने मूल स्वरूप से भटका नजर आता है। भारत में पश्चिमी चिकित्सा पद्धति या ऐलोपैथी अपने वैश्विक प्रभाव और त्वरित निदान के कारण आज भी प्रभावी है, जबकि पारम्परिक चिकित्सा अपने नए स्वरूप में योग, मेडिकल टूरिज्म ;चिकित्सा पर्यटनद्ध की ओर ज्यादा रूख कर रही है। पारम्परिक चिकित्सा पाठयक्रम में आधुनिक चिकित्सा के घटकों का प्रभुत्व होने से आयुष चिकित्सक भी एलोपैथी के अभ्यास की ओर जाने को प्रोत्साहित होते हैं। प्रत्येक प्रणाली के विकास के लिए समान नीतियां, समीक्षा और योजनाएं काम नहीं कर पा रहीं हैं, जिससे प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों का संयुक्त प्रशासन एकीकृत रूप से मजबूत नहीं है। पारम्परिक चिकित्सा पद्धति का आधुनिकीकरणः औषधीय पौधों पर आधारित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ और पारंपरिक रूप से प्राप्त दवाओं से विकासशील देशों में विशेष रूप से आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। आधुनिक तकनीकें, जैसे कि आर्टिपिफशियल इंटेलिजेंस ;एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्ध स्क्रीनिंग का उपयोग, पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य और रुझानों को मैप करने और पफार्माकोकाइनेटिक गुणों के लिए प्राकृतिक उत्पादों की जांच करने में, मोबाइल पफोन ऐप, आॅनलाइन कक्षाओं और अन्य प्रौद्योगिकियों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को भी अद्यतन किया गया है। अध्ययन के तरीकों का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि और विश्राम प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए होता है, जो ध्यान और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा उपचार का हिस्सा है, तथा तनावपूर्ण समय में मानसिक स्वास्थ्य में तेजी से सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। जडी-बूटी और पारम्परिक दवाओं के साथ, हम अच्छी तरह से नियंत्रित परीक्षणों में उपचार की शक्ति, प्रभावकारिता, नियंत्रित दवाओं और सुरक्षा की जांच करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और तकनीकी नवाचारों ने इसे आगे कर बुनियादी विज्ञान, नवाचार और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के साथ जोडकर आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे नैदानिक ज्ञान से लैस चिकित्सक, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा में मौजूदा और उभरते अंतरालों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें संबोधित कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आयुष में शोध मुख्य रूप से कुछ औषधीय पौधों/दवाओं के नैदानिक परीक्षण पर केंद्रित है, जबकि आहार और जीवनशैली में बदलाव को नजरअंदाज किया जाता है। परंतु अब ऐसा नहीं है, और बहुत से केंद्रों में कैम्प या अन्य माध्यमों से आहार के साथ योग विद्या और आयुर्वेद इत्यादि के साथ सुलभ उपचार सुविधा उपलब्ध है। भारत में पारम्परिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्रः विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ था। पारम्परिक चिकित्सा में एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक चिकित्सा और हर्बल मिश्रण जैसी प्राचीन प्रथाओं के साथ-साथ आधुनिक दवाएं भी शामिल हैं। पारंपरिक चिकित्सा उन विधियों पर निर्भर करती है, जो सावधानीपूर्वक तैयार किए गए परीक्षणों और शोधों के साथ सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई हैं। वर्ष 2012 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कई औद्योगिक देशों में लगभग आधी आबादी नियमित रूप से किसी न किसी रूप में पूरक और वैकल्पिक उपचारों ;ट्रैडिशिनल और काॅम्प्लीमेंटरी मेडिसिनद्ध का उपयोग करती है। जिसमें ,संयुक्त राज्य अमेरिका (42%)आस्ट्रेलिया (48%) ;प्फा(स (49ः%) (कनाडा (70%) (चिली (71%) (कोलंबिया (40%) और कुछ अप्रफीकी देशों में तो यह 80ः तक इस्तेमाल होती है, जबकि भारत में उपचार में ठोस शोध का अभाव है, जिसके आधार पर सही निर्णय, संभावित खतरे और लाभ अप्रमाणित हैं। भारत के जामनगर, गुजरात में ग्लोबल सेंटर पफाॅर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की घोषणा 03 नवंबर, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ;डब्ल्यूएचओद्ध के महानिदेशक डाॅ टेड्रोस घेब्रेयसस द्वारा की गई थी। इसका अंतरिम कार्यालय गुजरात में आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) के रूप में होगा। अपने बुनियादी और परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से लगभग 250 मिलियन अमेरीकी डाॅलर की निवेश सहायता मिलेगी। डाॅ. टेड्रोस एडनाॅम घेब्रेयसस ने अपने सम्बोधन में पारंपरिक औषधि के डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र को वास्तव में एक वैश्विक परियोजना बताया, और कहा कि यह केंद्र पारंपरिक औषधि के वादे को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। पारंपरिक औषधियों के उत्पाद ;प्राॅडक्ट्सद्ध विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में हैं। भारत पारंपरिक औषधि के अपने ज्ञान को दुनिया तक ले जाने में सक्षम होगा और इसी तरह दुनिया भी इस क्षेत्रा में भारत आएगी। भारत में इस केंद्र की स्थापना में उनके समर्थन के लिए उन्होंने प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। ‘‘भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जीवन का एक समग्र विज्ञान है’’ -प्रधानमंत्राी श्री नरेन्द्र मोदी पारम्परिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र का उद्देश्यरू अपनी तरह का पहला ज्ञान का यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा की प्रथाओं और उत्पादों पर गुणात्मक मानक स्थापित करने के लिए चार मुख्य रणनीतिक क्षेत्रों जैसेः- साक्ष्य और शिक्षण ;डेटा और विश्लेषणद्ध स्थिरता और समानता एवं वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास में पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को अनुकूलित करने में मदद करेगा। इसके साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, जैव विविधता इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करने तथा स्थानीय विरासत, संसाधनों और अधिकारों के सम्मान में भूमिका निभाएगा। इस वैश्विक केंद्र की स्थापना में 107 डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के सरकारी कार्यालयों के साथ पारम्परिक चिकित्सा के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों की परिकल्पना की गई हैः- ऽ पारंपरिक चिकित्सा में स्वास्थ्य सुविधाओं, कार्यरत कर्मचारियों और मान्यता प्राप्त संस्थानों का एकीकरण करना। ऽ पारम्परिक ज्ञान डेटाबेस प्रणाली के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ऽ पारम्परिक चिकित्सा में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के घटकों में 40ः प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, इसलिए इसके पोषण और जैव विविधता के संरक्षण की ओर ध्यान देना। ऽ पारम्परिक औषधियों की स्वीकार्यता में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों क आधार पर इन औषधियों का परीक्षण और प्रमाणन करने की योजना ऽ साक्ष्य आधारित मानचित्राण में आर्टिपिफशियल इंटेलिजेंस ;कृत्रिम बु(िमत्ताद्ध का उपयोग और पारंपरिक चिकित्सा में प्रयुक्त प(तियों के नवप्रवर्तन को ब यह केंद्र विश्व के पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए एक मंच के रूप मे कार्य करेगा जहां वह एक साथ मिलकर औषधी ;दवाइयांद्ध विकसित करने में अपने अनुभव का उपयोग कर सकेंगे। ऽ केंद्र पारंपरिक औषधियों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु धन जुटाने में सक्षम होगा। ऽ किसी भी रोगी को पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की दवाओं से लाभान्वित करने के लिए यह केंद्र विशिष्ट रोगों के लिए समग्र उपचार प्रोटोकाॅल तैयार करने में मदद कर सकता है। वर्तमान में उपयोग आने वाली लगभग 40ः स्वीकृत दवा उत्पाद प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। एस्पिरिन की खोज विलो पेड़ की छाल का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा के पफार्मूलों पर आधारित है। गर्भनिरोधक गोली जंगली रतालू के पौधों की जड़ों से विकसित की गई थी। बच्चों के कैंसर के उपचार गुलाबी पेरीविंकल पर आधारित है। इसी प्रकार मलेरिया रोग के नियंत्राण के लिए आर्टेमिसिनिन पर नोबेल पुरस्कार विजेता शोध प्राचीन चीनी चिकित्सा ग्रंथों की समीक्षा के साथ शुरू हुआ माना जाता है। भारत में भी औषधीय पौधों पर कई महत्वपूणर्् ा अनुसंधान कार्य हुए हैं। लखनऊ में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधी एवं सगंध पौधा संस्थान तथा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में औषधीय पौधों से सम्बंधित कई उत्पाद और ‘सहेली गर्भनिरोधक गोली’ जैसी कई प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां हासिल की गई हैं। देश में कई अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्राीय संस्थानों द्वारा भी पादप औषधि के क्षेत्रा में बहुत अधिक कार्य किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ;डब्ल्यूएचओद्ध का पारंपरिक चिकित्सा का यह भारतीय वैश्विक केंद्र आने वाले समय में ना केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इस वैश्विक केंद के शुरू होने पर भारत में भी पारम्परिक चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान को वैश्विक स्तर पर और अधिक बढावा, मान्यता और विशेष रूप से सम्मान प्राप्त होगा।